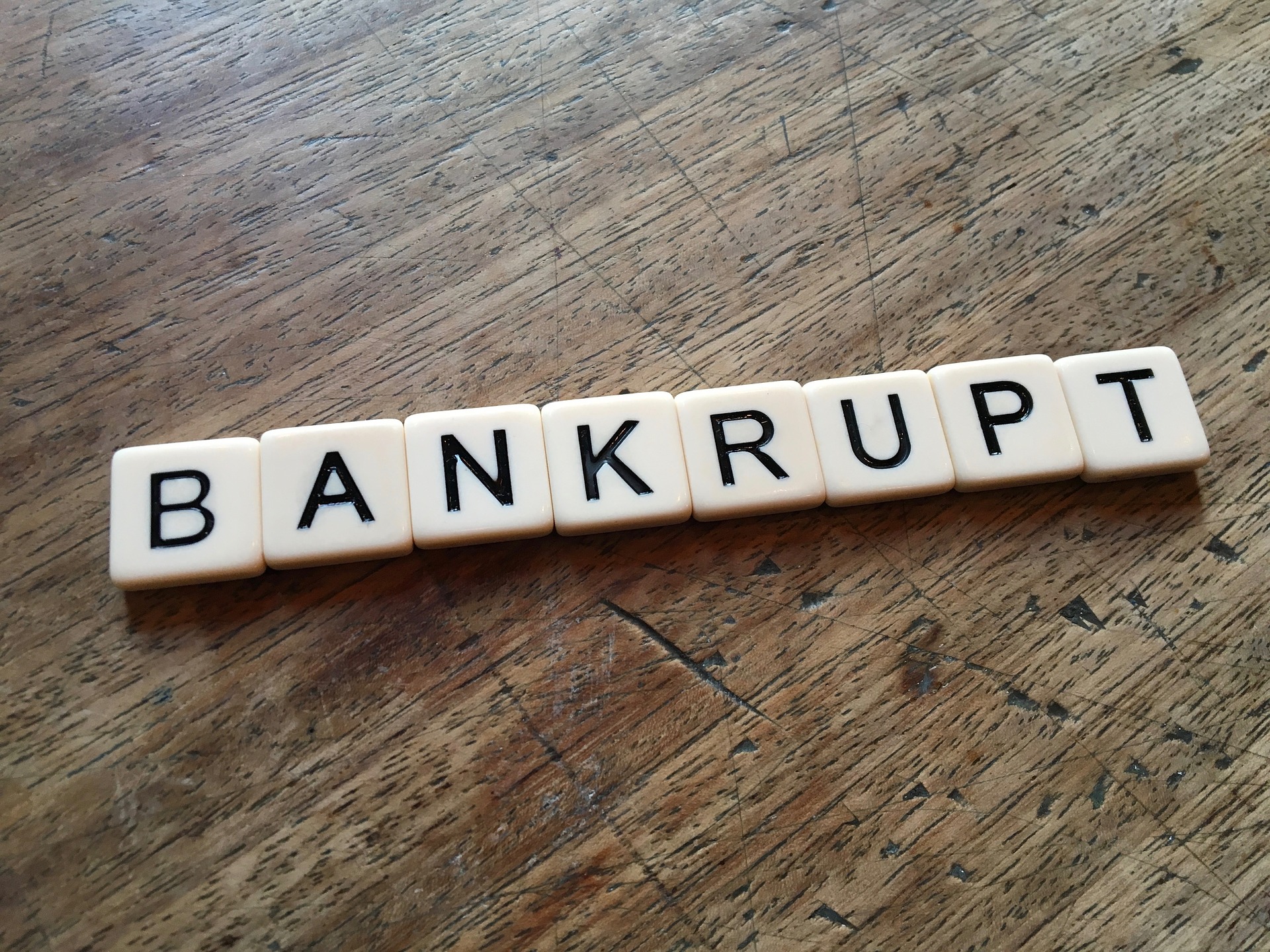पिछले साल सरकार ने जरूरत पड़ने पर कंपनी को दिवालिया घोषित करने के लिए खास कानून बनाया था. इसके तहत भारतीय दिवालियापन बोर्ड की स्थापना की गई थी. हाल ही में इस बोर्ड ने कहा है कि उसने जनता से बैंक्रप्सी कोड, 2016 के तहत अधिसूचित नियमों में बदलाव के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं.
लोग 31 दिसंबर, 2018 तक अपने विचार साझा कर सकते हैं. बोर्ड ने बताया है कि जनता से प्राप्त सुझावों के आधार पर अधिनियम में बदलाव किए जाएंगे.
इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आईबीसी) के अंतर्गत बना बोर्ड हाल ही में मीडिया से मुखातिब हुआ. इसने कंपनी को दिवालिया घोषित करने के कानून से जुड़ी कुछ अहम बातों के बारे में बताया. इसके अनुसार, आरबीआई ने पिछले साल 12 बड़ी कंपनियों से कर्ज वसूलने की शुरुआत की थी.
इन 12 कंपनियों पर कुल 2,36,483 करोड़ रुपये का कर्ज था. नए कानून की मदद से ही भूषण स्टील का टाटा स्टील अधिग्रहण कर सकी. टाटा स्टील ने भूषण स्टील की 72 फीसदी हिस्सेदारी 36,400 करोड़ में खरीदी है.
केंद्र सरकार ने आर्थिक सुधारों की दिशा में काफी कदम उठाए हैं. इस कानून को सरकार की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है. सरकार ने बीते शीतकालीन सत्र में ‘इनसॉल्वेंसी एवं बैंकरप्सी संशोधन विधेयक, 2017’ को लोकसभा में पारित कराया था.
तब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि ‘इनसॉल्वेंसी एवं बैंकरप्सी संशोधन विधेयक, 2017’ पुराने ‘इनसॉल्वेंसी एवं बैंकरप्सी संशोधन विधेयक, 2016’ की जगह लेगा.
इसमें कर्ज न चुकाने वाले बकाएदारों को अपनी खुद की ही संपत्ति की निलामी एवं बोली लगाने से रोका गया है. पुराने बिल में ये स्पष्ट नहीं था कि विवादों में फंसी संपत्तियों की बोली लगाने का अधिकार किसको हैॽ इसकी प्रक्रिया क्या होगीॽ इस परिस्थिति में बोली कौन लगा सकता हैॽ कौन नहीं लगा सकता हैॽ
सरकार ने इन्हीं खामियों को ध्यान में रखते हुए तब संशोधन किया था. साथ ही स्पष्ट किया था कि दिवालिया हो चुका व्यक्ति या संस्था अपनी खुद की संपत्तियों की बोली नहीं लगवा सकता है.
भारत में वर्ष 2016 से पहले कोर्इ भी ऐसा कानून नहीं था जो ‘इनसॉल्वेंसी एवं बैंक्रप्सी’ को एक साथ परिभाषित करता हो. पहले इसे परिभाषित करने के लिए लगभग 12 कानूनों का इस्तेमाल किया जाता था.
उसमें से कुछ तो 100 साल से भी अधिक पुराने हो चुके थे. पहले ‘इनसॉल्वेन्सी एवं बैंकरप्सी” को परिभाषित करने के लिए 1909 के ‘प्रेसिडेंसी टाउन इनसॉल्वेंसी एक्ट’ और ‘प्रोविंशियल इनसॉल्वेंसी एक्ट 1920’ इत्यादि जैसे कानूनों को उपयोग में लाया जाता था.
पूर्व कानून सचिव टी.के. विश्वनाथ की अध्यक्षता में बनी समिति ने दिवालिया घोषित करने के कानून को बनाने की सिफारिश की थी. इस समिति ने 4 नवंबर, 2015 को कानून का प्रारूप वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपा था. समिति ने कंपनी के दिवालिया होने की स्थिति में प्रमोटरों के नियंत्रण पर लगाम लगाने की सिफारिश की थी. समिति के अनुसार, दिवालिया होने के बाद सिर्फ 20 फीसदी कर्ज की ही वसूली हो पाती थी.
इस समिति ने कंपनी के दिवालिया होने की स्थिति में मामले को सुलझाने के लिए 180 दिन की अधिकतम सीमा तय करने की सिफारिश की थी. वर्तमान कानून में 180 दिन के साथ ही 90 दिन की रियायत का भी प्रवधान है.
इस बीच कॉरपोरेट लोन के रूप में बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है. एनपीए की दर और बोर्ड के काम करने की रफ्तार में अभी बड़ा अंतर दिख रहा है. बोर्ड को तेजी से दिवालिया हो रहे कॉरपोरेट के मामलों को निपटाना होगा.
विक्रान्त सिंह
संस्थापक एवं अध्यक्ष, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स थिंक काउन्सिल, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी.